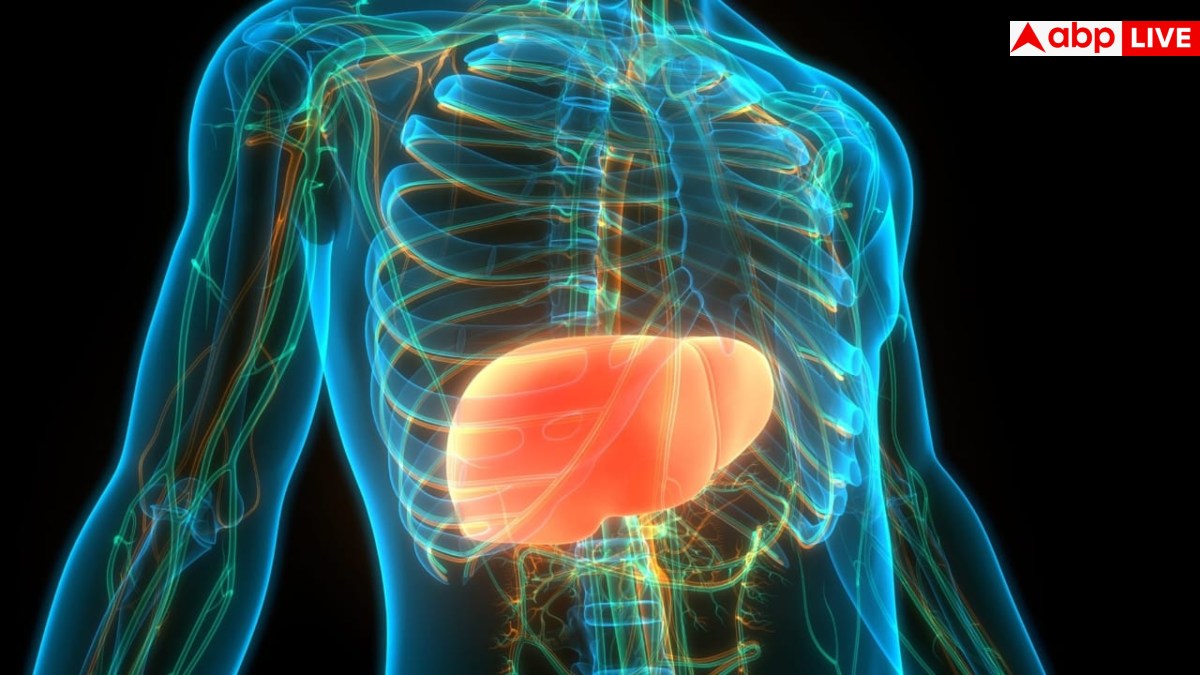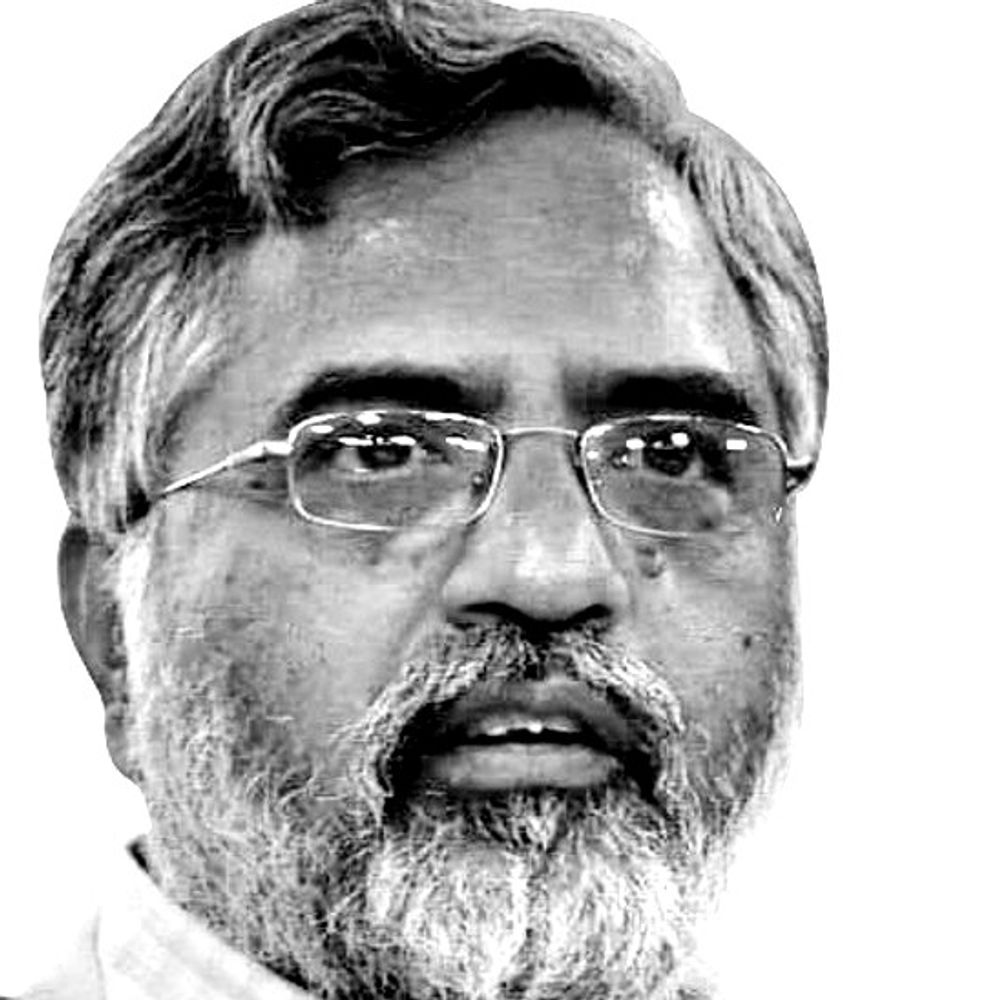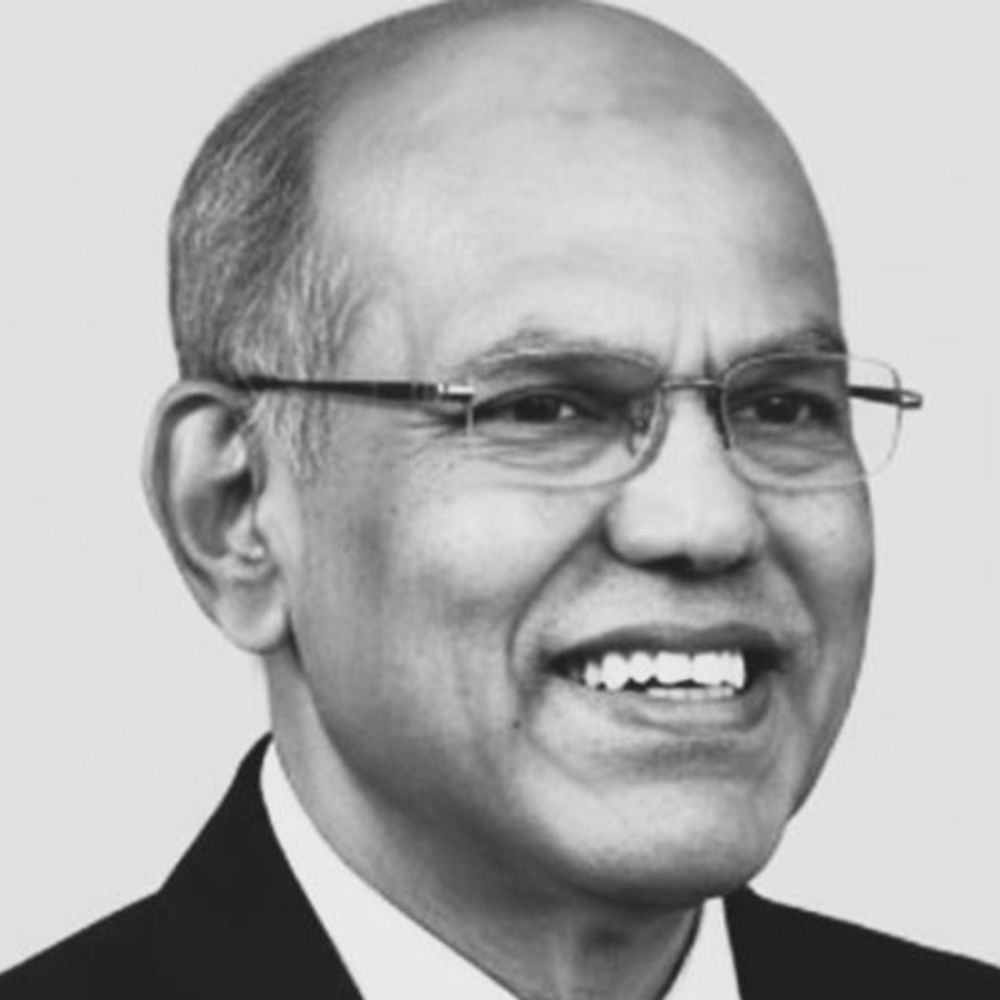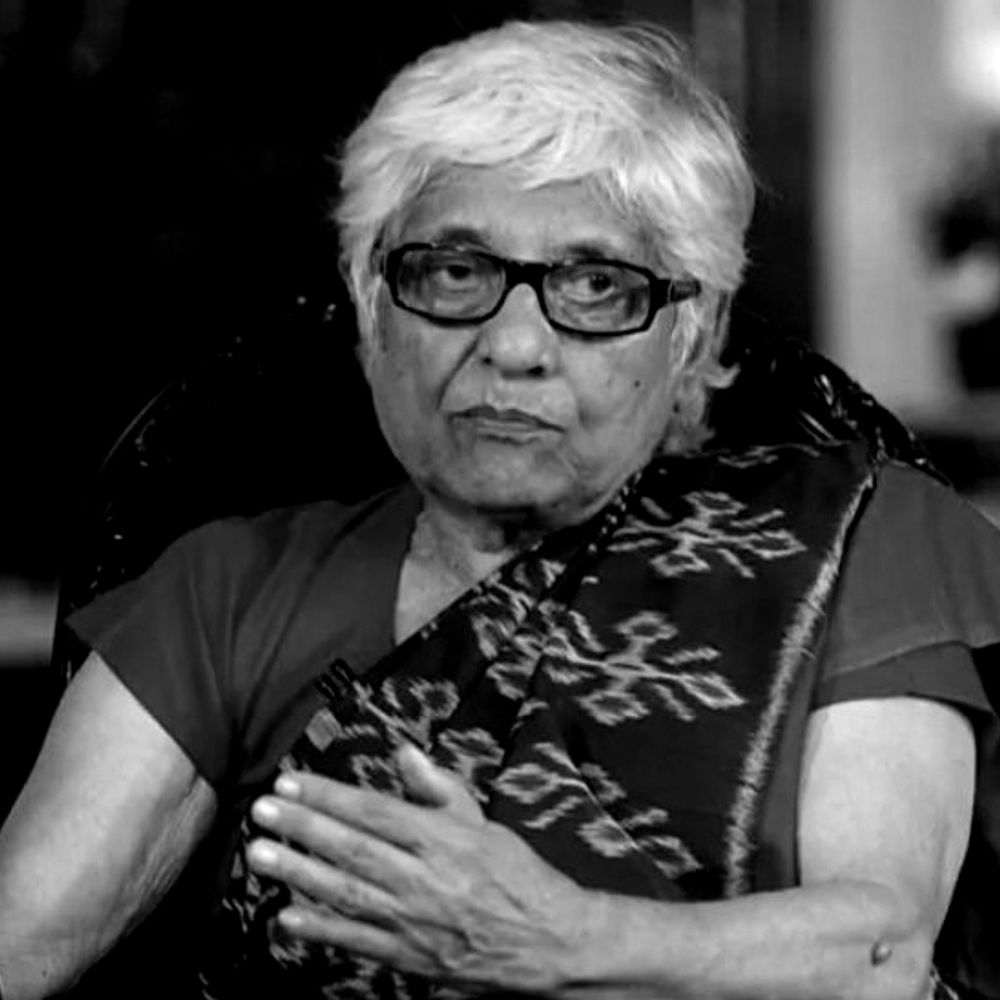We use cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. By clicking “Allow All Cookies”, you agree to our use of cookies.
- Hindi News
- Opinion
- Prof. Chetan Singh Solanki’s Column Diwali Firecrackers Are Visible, But What About The Invisible Pollution Of Everyday Life?
-
कॉपी लिंक
हर दिवाली जब घरों में दीये जगमगाते हैं और रात के आसमान में पटाखों की धमक और रौनक फैल जाती है, तो एक जानी-पहचानी बहस फिर से शुरू हो जाती है- हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं? न्यूज एंकर, एक्टिविस्ट और यहां तक कि अदालतें भी इस पर अपनी राय देती हैं। एक रात के लिए पूरा देश प्रदूषण पर ध्यान देने लगता है, मानो हमारी सामूहिक पर्यावरणीय चेतना सोने से पहले थोड़ी देर के लिए जाग जाती है। हम बात करते हैं, बहस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
सच्चाई तो ये है कि केवल एक दिन की दिवाली के पटाखे हमारा दम नहीं घोंटते, बाकी के जो 364 दिन हैं, उनके कारण हमारा पर्यावरण बदलता है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग दो मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अगर इसे हमारे 1.4 अरब लोगों से गुणा करें, तो आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा मिलेगा- हम सालाना अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।
अब इसकी तुलना दिवाली की रात फोड़ने वाले सभी पटाखों से होने वाले अनुमानित उत्सर्जन से करें। अगर हर भारतीय घंटों पटाखे जलाए, तब भी यह कुल उत्सर्जन एक छोटा-सा अंश ही होगा- शायद दिल्ली के यातायात उत्सर्जन के एक दिन से भी कम!
धुआं और शोर तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम अकसर उस अदृश्य प्रदूषण को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी कारों, एयर कंडीशनर, बिजली की खपत करने वाले उपकरणों, आयातित उत्पादों और हमारे आधुनिक जीवन की सुख-सुविधाओं के कारण लगातार बढ़ते उपभोग से उत्पन्न होता है। ये अदृश्य उत्सर्जन दिवाली की रात होने वाले उत्सर्जन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होता है।
हर बार जब हम एसी चालू करते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, कोई नया गैजेट खरीदते हैं या कपड़ों की सेल में एक की जगह दो जोड़ कपड़े खरीदते हैं, तो हम चुपचाप, अदृश्य पटाखे फोड़ते हैं। ये अदृश्य पटाखे कार्बन उत्सर्जन के ऐसे विस्फोट होते हैं, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु इनका असर हमारे पर्यावरण पर सैकड़ों सालों तक रहता है।
दिवाली के पटाखों के दिखने वाले धुएं के विपरीत- जो कुछ घंटों में साफ हो जाता है- यह अदृश्य उत्सर्जन हर दिन, जाने-अनजाने जमा होता जा रहा है। इस कारण धरती पर जलवायु परिवर्तन हो गया है। पृथ्वी अब धीरे-धीरे गर्म होती जा रही है और पूरा मौसम-चक्र बदल चुका है।
असहज करने वाली सच्चाई यह है कि लगभग 85 प्रतिशत रोजमर्रा की मानवीय गतिविधियां- बिजली उत्पादन से लेकर परिवहन, उद्योग और खाना पकाना- यह सब जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में सुविधा का लगभग हर कार्य कार्बन उत्सर्जन के कारण ही संभव हो पाता है। एक तरह से कहें तो हमारे दैनिक जीवन के 85% प्रतिशत कार्यों के द्वारा हम लगभग दिन के 85% समय अदृश्य पटाखे फोड़ते हैं।
इसलिए जब हम वायु प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों की निंदा करते हैं, तो हमें अपनी उन दैनिक आदतों की भी निंदा करनी होगी, जो वातावरण को सैकड़ों वर्षों के लिए प्रदूषित करती हैं। समस्या दिवाली की एक रात की खुशी नहीं, सालभर चलने वाला अति उपभोग का त्योहार है।
सच यही है कि जलवायु परिवर्तन कुछ असाधारण घटनाओं से नहीं होता- यह अरबों लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या से होता है। त्रासदी यह नहीं है कि लोग साल में एक बार पटाखे फोड़ते हैं, बल्कि यह है कि हम अनजाने में हर घंटे कार्बन जलाते हैं।
आधुनिक जीवनशैली ने हर क्रिया- खाना, घूमना, खरीदना, यहां तक कि जश्न मनाने को भी कार्बन उत्सर्जन यानी अदृश्य पटाखों के विस्फोट में बदल दिया है। हमारी सुविधाएं और हमारी अत्यधिक जरूरतें एक तर्ज से शांत विस्फोटक बन गई हैं।
दिवाली जैसे त्योहार एक आईना हैं। ये बताते हैं कि हम कौन हैं। एक ऐसा समाज- जो दिखाई देने वाले धुएं पर प्रतिक्रिया करता है और अदृश्य नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। हमें एक दिन के संयम नहीं, साल भर चलने वाली जाग्रति की जरूरत है। जीवन का हर दिन सचेतन होना चाहिए, तभी हमारी हर दिवाली वास्तव में प्रकाश का उत्सव होगी- न केवल हमारे लिए, बल्कि इस ग्रह के लिए भी। (ये लेखक के निजी विचार हैं)
-
एन. रघुरामन का कॉलम: गांवों में पटाखे तरह-तरह की मिट्टी की खुशबू लेकर आते हैं!
-
श्लोमो बेन-एमी का कॉलम: इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद गाजा में किसकी जीत हुई?
-
पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम: वृद्धावस्था में रिश्तों की पूंजी का भी संग्रह शुरू कर दें
-
संजय कुमार का कॉलम: बिहार चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है