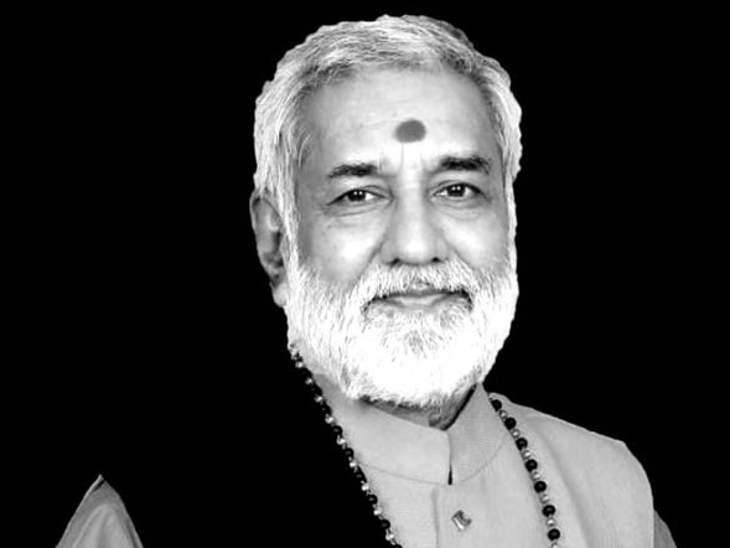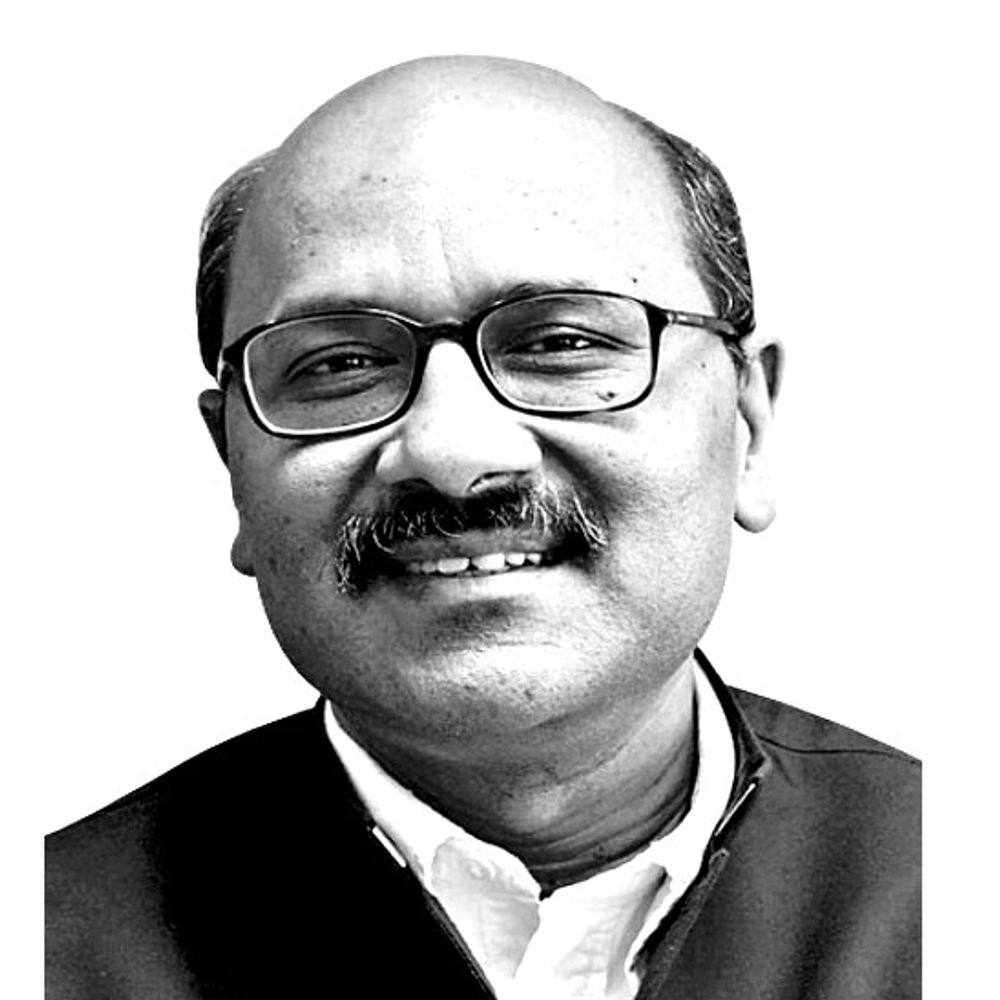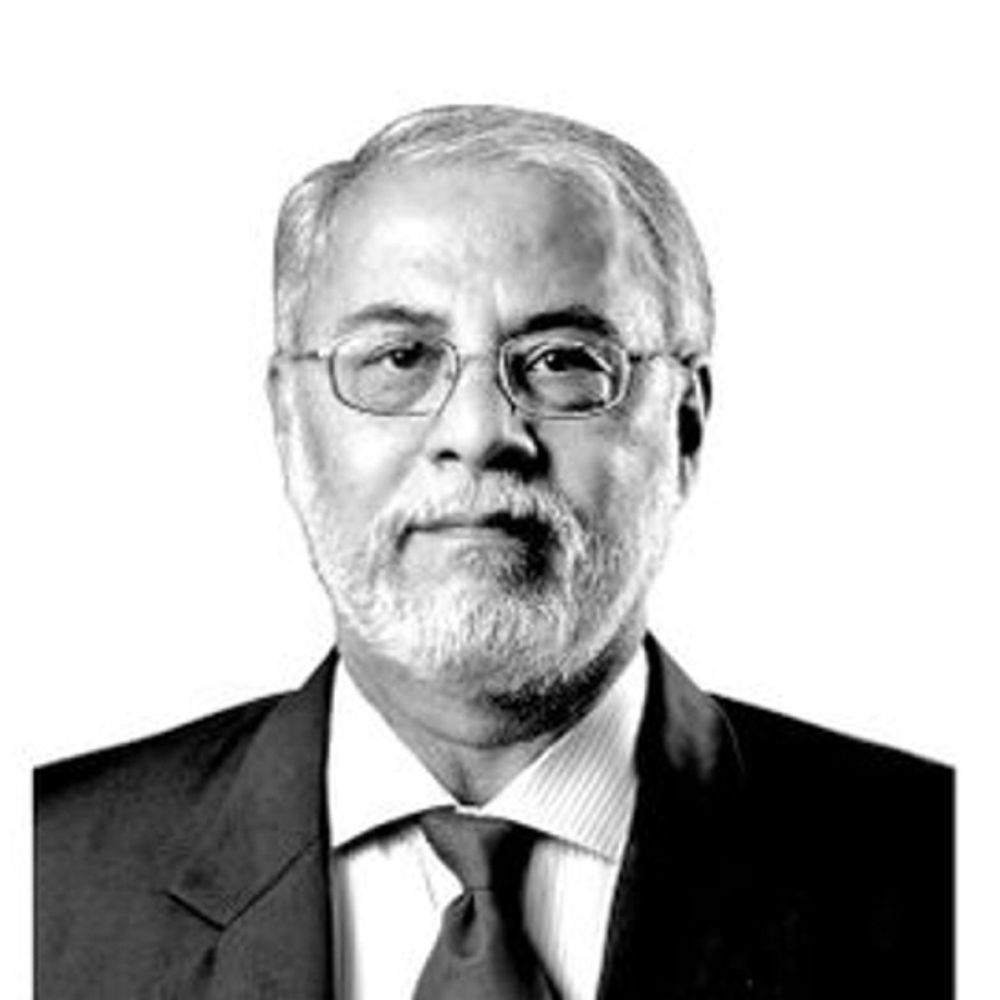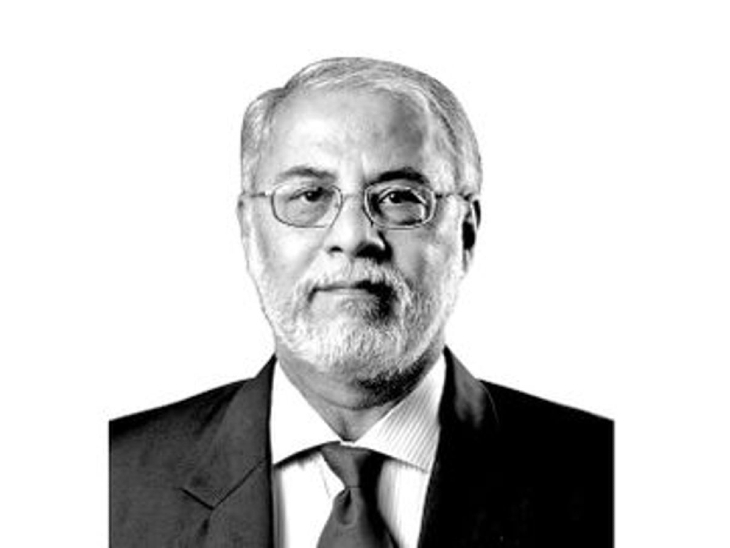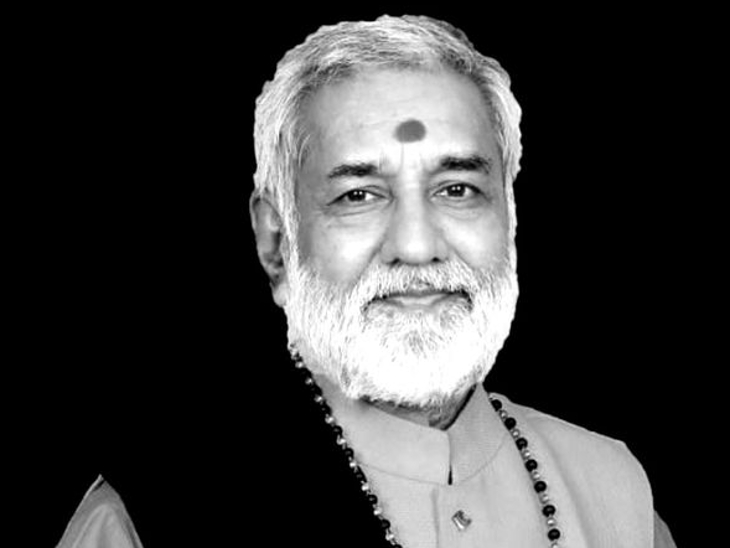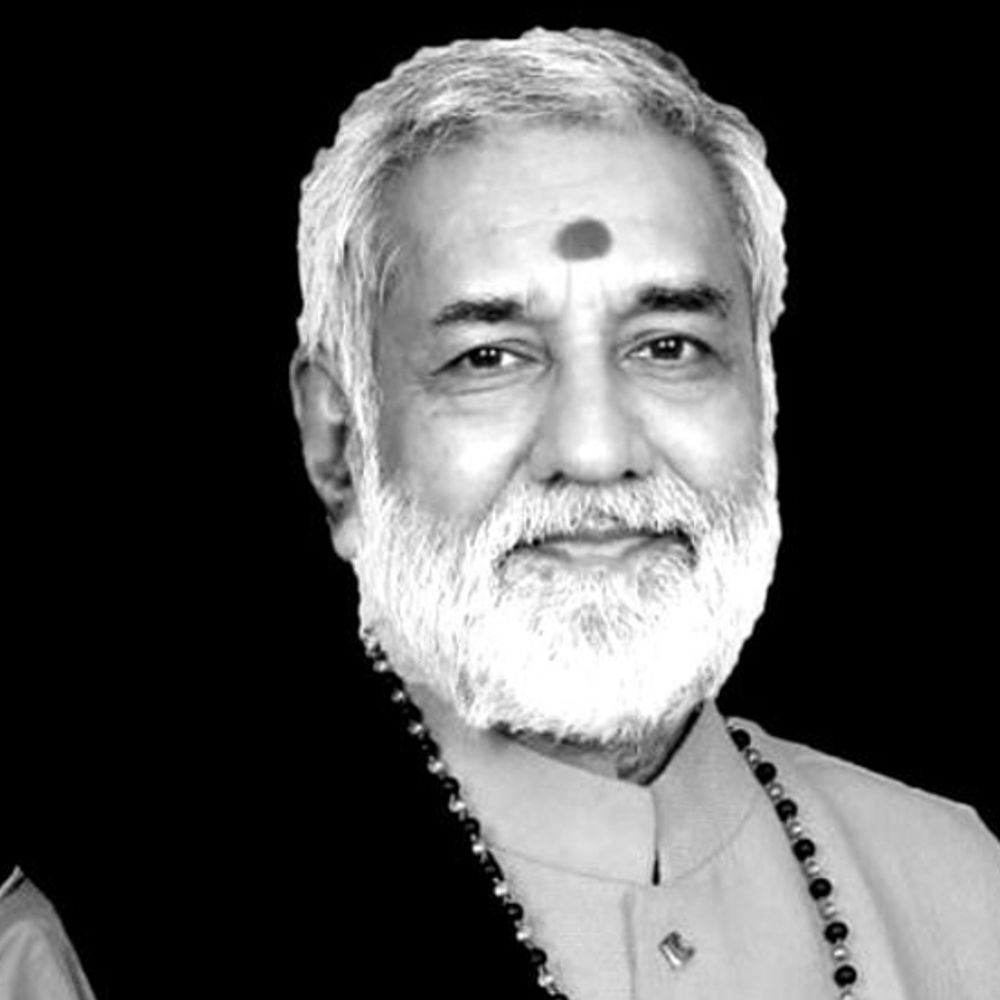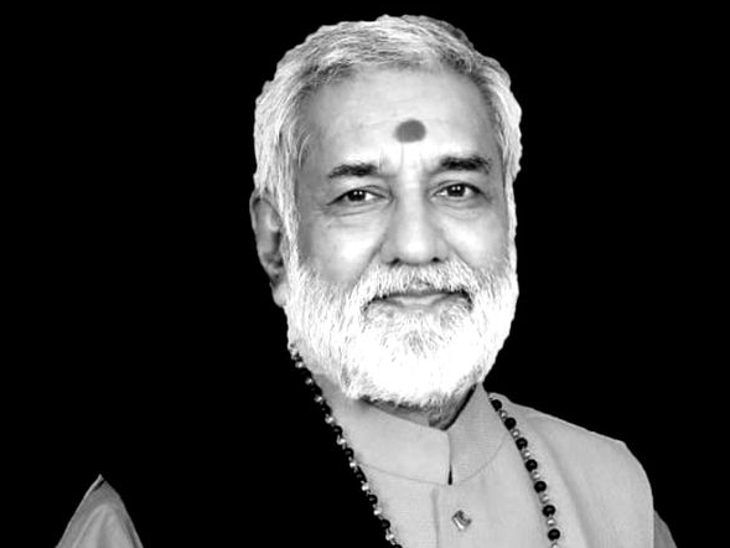- Hindi News
- Opinion
- Shekhar Gupta’s Column: The Film ‘Homebound’ Teaches A Lesson
शेखर गुप्ता का कॉलम:फिल्म ‘होमबाउंड’ एक सबक सिखाती है
-
कॉपी लिंक
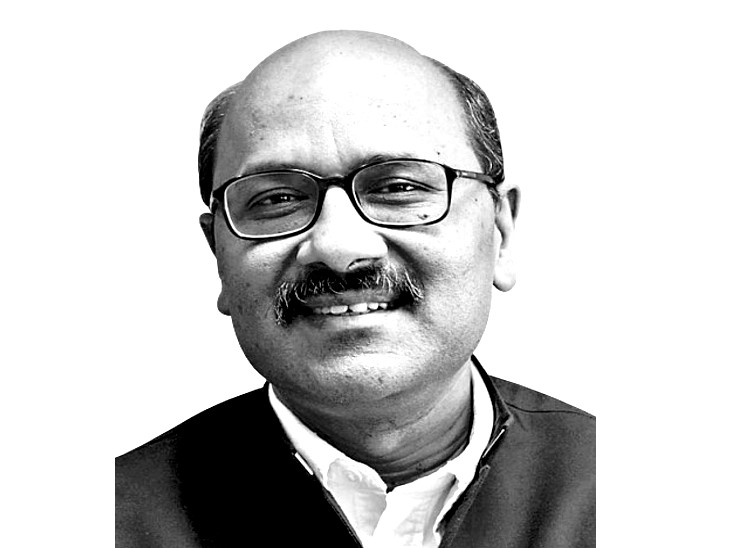
तीन बातों के मेल ने भारत में जातियों और अल्पसंख्यकों से जुड़े ऐसे मसले उभारे हैं, जिन्हें वह संविधान निर्माण के 75 साल बीत जाने के बाद भी हल करने में विफल रहा है। ये तीन बातें हैं- भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश पर उनकी ही अदालत में जूता फेंका गया; हरियाणा में एक दलित आईपीएस अफसर ने खुद को गोली मार कर खुदकशी कर ली और यह आक्रोश भरा नोट लिख गए कि किस तरह वर्षों से उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा और उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा और बॉलीवुड के प्रभावशाली फिल्म निर्माता नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ समृद्ध लोगों के बीच भी विरोधाभासी रूप से काफी सफल रही।
वैसे, यह फिल्म ‘सैयारा’, ‘पठान’, ‘जवान’, ‘एनिमल’, ‘बाहुबली’ या ‘कांतारा’ जितनी हिट नहीं रही। इसे 100 करोड़ की ‘ओपनिंग’ की सोचकर नहीं बनाया गया था। फिर भी धीमी शुरुआत के बाद इसने बातों-बातों में रफ्तार पकड़ ली- खासकर प्रोफेशनलों के ऊंचे तबके और आठ अंकों में वार्षिक पैकेज पाने वाले युवा उद्यमियों, सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग की आपसी बातचीत के जरिए।
इसका प्रमाण है इसकी स्क्रीनिंग के दौरान महानगरों में मल्टीप्लेक्सों के खचाखच भरे छोटे और महंगे हॉल। इन समूहों में जो ‘सोशल’ गप्पें होती हैं, उनमें मैंने नहीं सुना कि फिल्म उबाऊ, बड़बोली, राजनीतिक है। या यह कि आरक्षण ने असमानता दूर नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं?
इसके विपरीत, आप पाएंगे कि ‘होमबाउंड’ के दर्शक ग्रामीण भारत के तीन गरीब, पढ़े-लिखे, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी युवा किरदारों के संघर्ष से सहानुभूति रखते हैं। दर्शक इस बात को कबूल करते हैं कि यह ‘सिस्टम’ इन युवाओं को किस तरह धोखा देने के लिए ही बना है। तो हम क्या करें?
ध्यान रहे कि ये तीनों युवा भारत की एक तिहाई आबादी, दलितों और मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। शिक्षा, आरक्षण और सरकारी नौकरी समता और सम्मान दिलाने के लिए है, लेकिन हम इससे कितने दूर हैं, यह सीजेआई और हरियाणा के एडीजीपी की घटनाओं से साफ है। अगर एक मुख्य न्यायाधीश, आइपीएस, आईएएस अधिकारी को सम्मान और समता नहीं मिलती तो जााहिर है कि हमारी व्यवस्थागत नाइंसाफियां और पूर्वग्रह इतने गहरे धंसे हैं कि 75 वर्षों की आरक्षण व्यवस्था से भी दूर नहीं हुए हैं।
‘होमबाउंड’ के तीन दोस्त- चंदन कुमार (वाल्मीकि समाज के), मोहम्मद शोएब अली (मुस्लिम) और सुधा भारती (दलित)- पुलिस सिपाही की नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनकी भूमिका क्रमशः विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर ने निभाई है।
इस कहानी ने मुझे बाबू जगजीवन राम से 1985 में हुई बातचीत की याद दिला दी, जब मैंने अगड़ी जातियों के पहले आरक्षण विरोधी आंदोलन के बारे में ‘इंडिया टुडे’ के लिए रिपोर्टिंग करते हुए उनका इंटरव्यू लिया था। उस आंदोलन ने मंडल कमीशन को फिर से चर्चा में ला दिया था। जगजीवन राम सत्ता में नहीं थे और उनके पास बात करने के लिए वक्त भी था। उन्होंने आरक्षण के पक्ष में सबसे जोरदार तर्क प्रस्तुत किए थे।
उन्होंने आगरा के अपने एक पुराने मित्र, अनुसूचित जाति (तब दलित शब्द चलन में नहीं था) के जूता उद्यमी की कहानी बताई थी। उनके यह दोस्त करोड़ों के मालिक थे। फिर भी वे जगजीवन राम से विनती कर रहे थे कि वे उनके बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई की नौकरी लगवा दें।
बाबूजी ने उनसे कहा कि आपके पास इतनी दौलत है, आप अपने बेटे को एक मामूली एएसआई क्यों बनाना चाहते हैं? उनका जवाब था : ‘मैं कितना भी अमीर क्यों न हो जाऊं, कोई ब्राह्मण मेरे बेटे को इज्जत नहीं देगा, लेकिन वह एक एएसआई बन गया तो ब्राह्मण समेत सारे जूनियर उसे सलाम करेंगे’।
‘होमबाउंड’ फिल्म में तस्वीर थोड़ी पेचीदा है। चंदन सामान्य कोटे से परीक्षा देना चाहता है। उसका कहना है कि अगर उसने यह जाहिर कर दिया कि वह वाल्मीकि समाज से है, तो पुलिस महकमे में वे लोग उसे सफाई कर्मचारी बना देंगे। सुधा ग्रेजुएट बनने के बाद यूपीएससी की परीक्षा देना चाहती है और शोएब इतना स्मार्ट है कि घरेलू सामान की कंपनी में चपरासी की नौकरी करने के बावजूद बिक्री करवाने में अपने टाईधारी मैनेजरों को भी पीछे छोड़ देता है।
उसका ‘बिग बॉस’ उसके काम से हैरान है और उसे ‘बेचू’ कहकर बुलाता है, जो कुछ भी बेचने में माहिर है। शोएब भी टाईधारी मैनेजर बनने वाला है कि तभी बॉस के घर में एक पार्टी में नशे में धुत लोग क्रिकेट मैच देखते हुए उसे अपमानित करते हैं। वह भी खुशी मना रहा होता है, लेकिन उसका मखौल उड़ाते हुए पूछा जाता है कि उसका दिल तो टूट गया होगा क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को हरा दिया?
दलित और मुसलमान, दोनों को उनके पैतृक अतीत के बोझ के नीचे परस्पर विपरीत तरीके से कुचला जाता है। दलितों को पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय का बोझ उठाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें प्रताड़ित करने वाली जातियों को खुद में बदलाव लाना चाहिए।
इसी तरह, मुसलमानों को अपने मुगल/अफगान/तुर्क पूर्वजों और जिन्ना के कारण बहुसंख्य हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों और हुकूमत का हिसाब चुकाना पड़ता है। यह दोमुंहा हथियार चंदन, शोएब और सुधा और एक तिहाई भारत की तकदीर पर मिलकर वार करता है।
इस फिल्म ने जनसांख्यिकी वाले पहलू को छुआ है, जिसे हम अक्सर असंवेदनशील और उग्र मानते हैं, लेकिन संयोग से यह वास्तविक जीवन की कहानियों से मेल खाती है, जिनमें भुक्तभोगी वे हैं, जिन्हें सबसे विशेषाधिकार प्राप्त पद मिले। मैं आपको भारत के पहले दलित सीजेआई केजी बालकृष्णन की नियुक्ति के दिन ही किए गए उनके अपमान की याद दिलाना चाहूंगा। इस प्रवृत्ति की हम अनदेखी नहीं कर सकते, खासकर तब जब यह तीन में से एक भारतीय को प्रभावित करती हो।
एक तिहाई भारत की तकदीर पर मिलकर वार… दलितों को पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय का बोझ उठाना पड़ता है। इसी तरह, मुसलमानों को अपने मुगल/अफगान/ तुर्क पूर्वजों के अत्याचारों का हिसाब चुकाना पड़ता है। यह चंदन, शोएब और सुधा सहित एक तिहाई भारत की तकदीर पर मिलकर वार है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)
-
राजदीप सरदेसाई का कॉलम: सीजेआई पर फेंके जूते का निशाना न्याय व्यवस्था थी

-
नीरजा चौधरी का कॉलम: तालिबान को हमारी महिला- शक्ति का एहसास हुआ है

-
एन. रघुरामन का कॉलम: ‘री-कनेक्ट’ : जेन-जी ने निकाला बिना फोन के आपस में जुड़ने का नया तरीका

-
पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम: हर चीज के आरम्भ, मध्य और अंत में ईश्वर को रखें