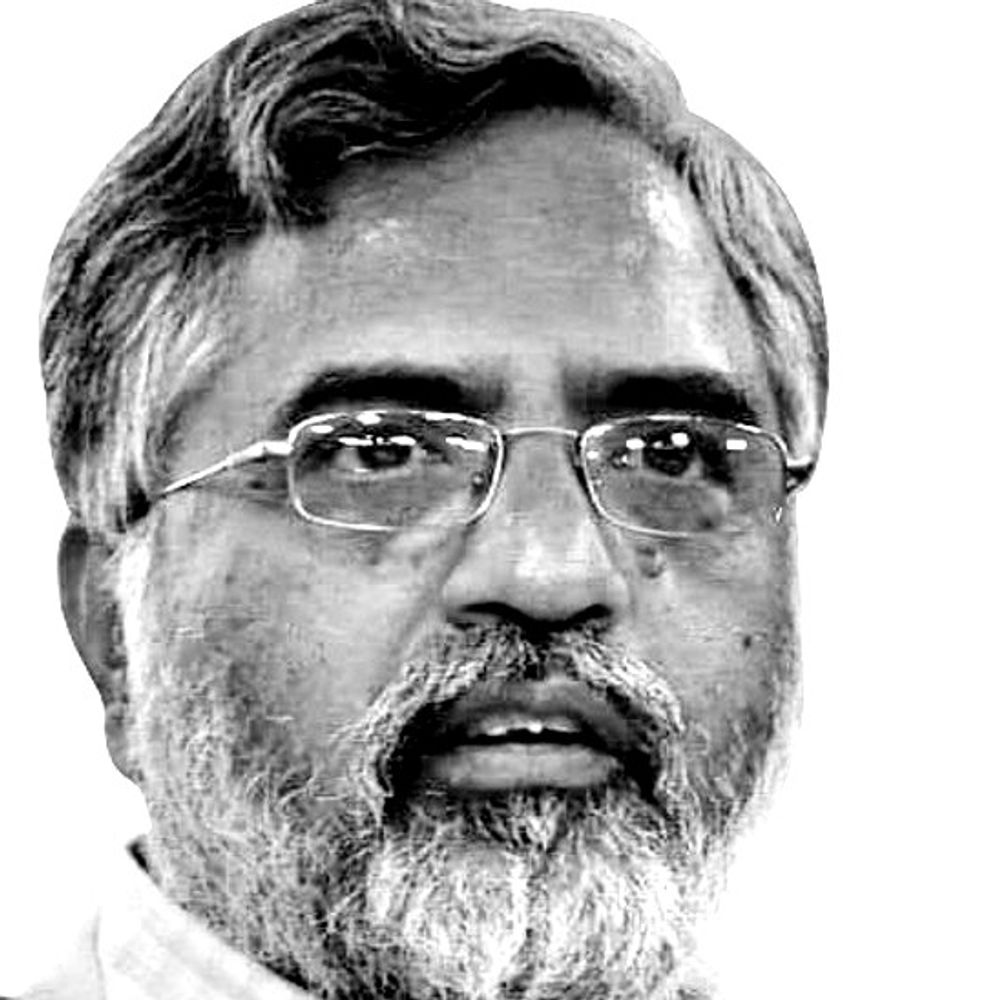प्रियदर्शन का कॉलम:वो असंतोष भी खत्म हो, जो हिंसा की ओर ले जाता है
- Hindi News
- Opinion
- Priyadarshan’s Column: May The Discontent That Leads To Violence Also End.
-
कॉपी लिंक
बीते दिनों माओवादी संगठनों से जुड़े कुछ बड़े नेताओं ने जैसे आत्मसमर्पण किया है, उससे लगता है सरकार अपने कहे मुताबिक अगले साल तक माओवाद के उन्मूलन में सफल हो जाएगी। लेकिन माओवाद का खात्मा जितना जरूरी है, उतना ही उन कारकों का भी है, जिनकी वजह से माओवाद पैदा होता है।
आखिर यह हाल की परिघटना नहीं है, देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग वर्षों में, अलग-अलग नामों से विकसित अति-वाम आंदोलन वह लाल गलियारा बनाते रहे हैं, जिसे मनमोहन से लेकर मोदी तक देश के लिए सबसे खतरनाक मानते रहे हैं।
निस्संदेह, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसक आंदोलनों की जगह नहीं हो सकती। अगर हम संसदीय लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो हिंसा के रास्ते का समर्थन नहीं कर सकते। वैसे भी हिंसा का अपना एक चरित्र होता है, जो बंदूक थामने वाले को भी बदल डालता है।
फिल्म ‘हाइवे’ का मार्मिक संवाद है- ‘जब एक गोली चलती है तो दो लोग मरते हैं- जिसे गोली लगती है, वह भी और जो गोली चलाता है वह भी।’ दुनिया भर की हिंसक क्रांतियों का अनुभव बताता है कि उनसे कहीं ज्यादा हिंसक व्यवस्थाएं निकली हैं।
फिर हिंसक आंदोलन अंततः राज्य की हिंसा को वैधता देते हैं। राज्य आज इतना शक्तिशाली है कि उसकी सत्ता को चे ग्वेरा के छापामार युद्धों वाली रणनीति से पलटा नहीं जा सकता। भारत जैसे विशाल राष्ट्र-राज्य के बारे में यह बात और सच है, जहां अपनी सारी विरूपताओं के बावजूद लोकतंत्र का वृक्ष इतना विराट हो चुका है कि वह अपरिहार्य लगता है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया के किसी भी आंदोलन या संघर्ष को बस दमन से नहीं कुचला जा सकता। भारतीय राष्ट्र-राज्य माओवाद को खत्म करे, यह जरूरी है, लेकिन माओवाद के पूरी तरह खात्मे के लिए जरूरी है कि वह असंतोष भी खत्म हो, जो युवाओं को इस राह की ओर ले जाता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि माओवाद के खात्मे की मुहिम की चपेट में बेगुनाह लोग न चले आएं, जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों में ‘को-लैटरल’ शिकार होते हैं।
दूसरी बात यह कि अंततः यह संघर्ष इस अंदेशे और सच्चाई से भी वैधता पाता है कि हमारे देश में दशकों से आदिवासियों के, गरीबों के अधिकार छीने गए हैं, उन्हें विस्थापित किया गया है, उनके रोजगार और उनकी आजीविका पर संकट बढ़ता गया है।
यह साफ है कि जिसे हम विकास कहते हैं, उसके फायदे सभी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ ने उसका बेतहाशा फायदा उठाया है और बहुत सारे लोग इसके लिए कुचले गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगल बहुत बड़ी आबादी के लिए जीवन का आधार ही नहीं रहे हैं, वे हिंदुस्तान के फेफड़े भी हैं, जो इसकी हवा साफ करते हैं, उसे सांस लिए जाने लायक बनाते हैं। अगर माओवाद के खात्मे के बाद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग-धंधों की विराट भट्टी में झोंक दिया गया, तो यह इन क्षेत्रों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
बच्चों के लिए स्कूल हों, बीमारों के लिए अस्पताल, नौजवानों के लिए कामकाज के अवसर और सभी वर्गों के लिए बराबरी और न्याय का आश्वासन- लोकतंत्र अपने न्यूनतम स्वरूप में इस आश्वासन का ही नाम है। लेकिन देश में यह आश्वासन कमजोर पड़ा है और जाति-धर्म-सम्प्रदाय- क्षेत्र के नाम पर विभाजनकारी राजनीति मजबूत हुई है।
माओवाद हो या असंतोष की दूसरी प्रवृत्तियां और अभिव्यक्तियां- इनको तभी समाप्त किया जा सकता है, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकें। लेकिन सुरक्षा बलों के सहारे माओवाद को खत्म करने के आत्मविश्वास और सरकारी तौर-तरीकों से असहमति रखने वालों को ‘अर्बन नक्सल’ करार देने की वैचारिकी- इन्हें छोड़ना भी नक्सल-मुक्त भारत बनाने के लिए जरूरी है।
किसी भी संघर्ष को बस दमन से नहीं कुचला जा सकता। यह भी ध्यान रखना होगा कि माओवाद के खात्मे की मुहिम की चपेट में बेगुनाह लोग न चले आएं, जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों में दोनों तरफ से ‘को-लैटरल’ शिकार होते हैं। (ये लेखक के निजी विचार हैं)
-
एन. रघुरामन का कॉलम: गांवों में पटाखे तरह-तरह की मिट्टी की खुशबू लेकर आते हैं!
-
श्लोमो बेन-एमी का कॉलम: इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद गाजा में किसकी जीत हुई?
-
पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम: वृद्धावस्था में रिश्तों की पूंजी का भी संग्रह शुरू कर दें
-
संजय कुमार का कॉलम: बिहार चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है