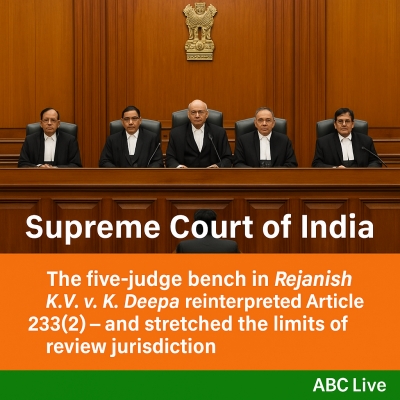समझाया: सुप्रीम कोर्ट ने रेजनीश केवी बनाम के. दीपा मामले में अनुच्छेद 145 का इस्तेमाल कैसे किया
रेजनीश केवी फैसले ने अनुच्छेद 233(2) के तहत पात्रता को स्पष्ट किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाओं का भी परीक्षण किया। एक समीक्षा याचिका में अनुच्छेद 145(3) का उपयोग करके, न्यायालय ने एक सुलझे हुए मुद्दे को एक नए संवैधानिक परीक्षण में बदल दिया।
- नई दिल्ली (एबीसी लाइव): हर कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चुपचाप न्यायिक शक्ति और प्रक्रियात्मक संयम के बीच संतुलन को बदल देता है। में हालिया संविधान पीठ का फैसला रेजनीश केवी बनाम के. दीपा ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मोड़ है.
जिला न्यायाधीश नियुक्तियों के लिए पात्रता पर विवाद के रूप में जो विवाद शुरू हुआ वह एक गहरे सवाल में बदल गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम निर्णयों की समीक्षा करते समय कितनी दूर तक जा सकता है। इस फैसले से यह विस्तार हुआ कि न्यायिक पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 137 और 145(3) के तहत न्यायालय की अपनी पहुंच का भी विस्तार हुआ।
यह व्याख्याकार बताता है कि कैसे न्यायालय ने उस मामले को फिर से खोलने के लिए एक समीक्षा याचिका का उपयोग किया जिस पर उसने पांच साल पहले ही निर्णय ले लिया था, यह न्यायिक अनुशासन और अंतिम निर्णय के लिए क्यों मायने रखता है, और आने वाले वर्षों में भारत की संवैधानिक वास्तुकला के लिए इसका क्या मतलब है।
पृष्ठभूमि: जब एक समीक्षा पुन: परीक्षण बन गई
22 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया रेजनीश केवी बनाम के. दीपा. मामले में संविधान के अनुच्छेद 233(2) की व्याख्या की गई, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है।
खंडपीठ ने कहा कि वकील और न्यायिक अधिकारी दोनों के रूप में सात साल का संयुक्त अनुभव वाला न्यायिक अधिकारी बार कोटा के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है।
ठोस परिणाम ने अवसर को व्यापक बनाया और भारत के बार-टू-बेंच मार्ग को आधुनिक बनाया। फिर भी प्रक्रिया असाधारण थी. न्यायालय ने अंतिम निर्णय फिर से खोला (धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय2020) और समीक्षा क्षेत्राधिकार के भीतर एक नई संवैधानिक सुनवाई को उचित ठहराने के लिए अनुच्छेद 145(3) का इस्तेमाल किया। इस विकल्प ने न्यायिक सुधार और पुनः मुकदमेबाजी के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया।
क्षेत्राधिकार संबंधी मोड़: से धीरज मोरे को रेजनीश के.वी **
यह मुद्दा 2018 में बार-कोटा पात्रता पर उच्च न्यायालय के परस्पर विरोधी विचारों के बाद उत्पन्न हुआ। दो जजों की बेंच में धीरज मोरे मुख्य न्यायाधीश से इसे बड़ी पीठ के पास भेजने को कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तब फैसला सुनाया कि सेवारत न्यायिक अधिकारी वकील के रूप में आवेदन नहीं कर सकते। यह फैसला पांच साल तक कायम रहा।
बाद में समीक्षा याचिकाओं में तर्क को नहीं बल्कि पीठ की संरचना को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संवैधानिक प्रश्न से जुड़े मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए थी। में रेजनीश के.वीसर्वोच्च न्यायालय ने उस दृष्टिकोण को स्वीकार किया और अनुच्छेद 145(3) लागू किया। ऐसा करके, इसने समीक्षा क्षेत्राधिकार का विस्तार किया और मामले को नए सिरे से सुना, जैसे कि एक नया संवैधानिक संदर्भ तय कर रहा हो।
अनुच्छेद 145(3): प्रक्रिया और शक्ति के बीच
अनुच्छेद 145(3) के अनुसार “संवैधानिक कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न” उठाने वाले किसी भी मामले की सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। फिर भी ऐसे रेफरल मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करते हैं, स्वचालित नियमों पर नहीं।
रेजनीश के.वी बेंच ने इस शक्ति की व्यापक रूप से व्याख्या की, जिससे तीन चिंताएँ पैदा हुईं:
ट्रिगर की गलत पहचान करना
धीरज मोरे आदेश में कभी भी अनुच्छेद 145(3) का उल्लेख नहीं किया गया। इसने केवल “उचित पीठ” की मांग की। इसे पूर्वव्यापी रूप से संविधान पीठ के संदर्भ के रूप में मानने से इसका अर्थ बदल जाता है और प्रक्रियात्मक निश्चितता कमजोर हो जाती है।
स्थापित कानून का विरोधाभास
पहले के मामले – जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम ठाकुर सिंह (1968) और भगवान स्वरूप लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) – यह स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 145(3) तभी लागू होता है जब कोई संवैधानिक प्रश्न अनसुलझा रहता है। एक अंतिम व्याख्या को “पर्याप्त प्रश्न” के नए लेबल के तहत दोबारा नहीं खोला जा सकता है।
धुंधली समीक्षा और उपचारात्मक क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 137 स्पष्ट त्रुटियों के लिए समीक्षा की अनुमति देता है। इसके विपरीत, उपचारात्मक याचिकाओं को परिभाषित किया गया है रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रे (2002), न्याय के दुर्लभ गर्भपात को संबोधित करने के लिए मौजूद है। उपचारात्मक क्षेत्राधिकार को लागू किए बिना पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करके, न्यायालय ने इन विशिष्ट शक्तियों का विलय कर दिया और अंतिम निर्णय को कमजोर कर दिया।
संस्थागत निहितार्थ: पुनः खुलने का भानुमती का पिटारा
ए. मिसाल अस्थिरता
अगर रेजनीश के.वी यह एक मिसाल है, संवैधानिक मुद्दों पर तीन-न्यायाधीशों के कई फैसलों को बेंच के आकार के लिए चुनौती दी जा सकती है। इस तरह के पूर्वप्रभावी दावे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अंतिमता को ख़त्म कर देंगे।
बी. न्याय तक पहुंच संबंधी चिंताएं
संविधान पीठ दुर्लभ और संसाधन-भारी हैं। यदि प्रत्येक “पर्याप्त प्रश्न” के लिए पांच न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तो लंबित संवैधानिक मामले बढ़ सकते हैं, जिससे न्याय वितरण धीमा हो सकता है।
सी. प्रशासनिक अनिश्चितता
यह फैसला मास्टर ऑफ रोस्टर सिद्धांत का भी परीक्षण करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश की पीठ के कार्यों को बाद में अमान्य घोषित किया जा सकता है, तो न्यायालय के भीतर प्रशासनिक स्थिरता ही तनाव में आ जाती है।
पंक्तियों के बीच पढ़ना: शुद्धता बनाम अंतिमता
समर्थकों का मानना है कि न्यायालय ने तकनीकी सीमाओं पर संवैधानिक सटीकता को प्राथमिकता दी। फिर भी ऐसा दृष्टिकोण सतर्कता को अतिरेक समझने में भ्रमित करता है।
मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या पाँच-न्यायाधीशों की व्याख्या सही है, बल्कि यह है कि क्या न्यायालय ने अपनी सीमाओं का सम्मान किया है। पुनः खोलने से धीरज मोरेइसने सुझाव दिया कि जब भी शुद्धता पर संदेह हो तो अंतिमता लचीली होती है। यह दृष्टिकोण संवैधानिक तर्क को मजबूत कर सकता है लेकिन न्यायिक प्राधिकरण के आधार – पूर्वानुमान को कमजोर करता है।
एबीसी लाइव इस व्याख्याता को अभी क्यों प्रकाशित कर रहा है
रेजनीश के.वी फैसला कोई नियमित नियुक्ति का मामला नहीं है. यह दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपनी सीमाओं को परिभाषित करता है और दो सिद्धांतों – अंतिमता और निष्पक्षता – को संतुलित करता है।
ऐसे समय में जब न्यायिक पारदर्शिता और संस्थागत अनुशासन सार्वजनिक जांच के अधीन है, अनुच्छेद 145(3) और 137 के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। यह निर्णय एक बड़े प्रश्न को आमंत्रित करता है: क्या संवैधानिक शुद्धता हमेशा न्यायिक अंतिमता पर हावी होनी चाहिए, और यह रेखा कौन खींचता है?